Wouldn’t such killing lead to chaos today? Isn’t Krishna’s insisting on in in the Gita also immoral?
Transcription: Narmada Shorewala Mataji (Kaithal)
प्रश्न: सम्पत्ति विवाद को लेकर लड़ा गया महाभारत का युद्ध क्या अनैतिक नहीं था? भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने संबंधियों की हत्या के लिए कहना क्या अनैतिक नहीं था? इस प्रकार यदि सब संपत्ति के लिए अपने संबंधियों की हत्या करने लगें, तो क्या इससे अव्यवस्था नहीं फैलेगी?
उत्तर: सर्वप्रथम, कौरवों और पाण्डवों के बीच जो विवाद था, वह केवल संपत्ति के लिए नहीं था- वह एक धार्मिक विवाद था। आरम्भ में संपत्ति अवश्य ही एक कारण था, लेकिन मुख्य कारण धार्मिक था। कौरवों और पाण्डवों की धर्म के प्रति निष्ठा अलग-अलग थी, जिसके कारण युद्ध हुआ।
इन सभी प्रश्नों का उत्तर धर्म के तीन अलग-अलग स्तरों पर समझा जा सकता है –
(i) एक क्षत्रिय का अपने लिये धर्म
(ii) एक क्षत्रिय का अपने नागरिकों के प्रति धर्म
(iii) एक क्षत्रिय का भगवद्भक्त के रूप में धर्म।
प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार क्षत्रियों का धर्म है शासन प्रदान करना। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि समाज के सभी वर्ग (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) अपना-अपना कर्तव्य निभायें, तो समाज का विकास सुसंगत और संतुलित होता है। इसी दृष्टिकोण से यदि एक क्षत्रिय अपने वर्ण के अनुसार शासन न करे और उनके पास शासन हेतु छोटा सा भी क्षेत्र न हो, तो उनका अपने धर्म के प्रति उल्लंघन होगा। हम जानते हैं कि पाण्डव युद्ध टालने के लिए अपने अधिकार की सारी संपत्ति त्यागने को तैयार थे। उन्होंने मात्र पांच गाँवों की ही मांग की थी। इससे स्पष्ट होता है कि पाण्डव भूमि और संपत्ति के लोभी नहीं थे। यदि ऐसा होता तो वे एक विशालकाय राज्य की तुलना में मात्र पाँच गाँव लेने के लिये कभी तैयार नहीं होते। साथ ही साथ श्रीकृष्ण को यदि सम्पत्ति के विषय को लेकर युद्ध के लिए उकसाना ही होता तो वे शांति दूत के नाते स्वयं पाँच गाँवों का प्रस्ताव कभी नहीं रखते।
दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार, क्षत्रियों का धर्म है कि वे अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें। महाभारत में हम देखते हैं कि युद्ध टालने के लिए पाण्डव अपनी ही पत्नी के प्रति किये गए अत्यंत शर्मनाक और अपमानजनक व्यवहार को भी क्षमा करने के लिए तैयार थे। किन्तु दुर्योधन, हालाँकि उसमें कुछ लक्षण क्षत्रियों के थे, पर मुख्यतः वह एक आसुरी स्वभाव का व्यक्ति था। ऐसा राजा यदि नागरिकों को कभी न्यायपूर्ण शासन नहीं दे सकता। अतः एक क्षत्रिय होने के नाते पाण्डवों का यह कर्तव्य था कि वे अपने नागरिकों को एक न्यायपूर्ण राजा प्रदान करें।
महाभारत में दिए गए श्लोकों के आधार पर कुछ विद्वानों व इतिहासकारों का मत दुर्योधन को लेकर अलग-अलग हैं। कुछ के अनुसार दुर्योधन एक अत्यंत बुरा राजा था, किन्तु अन्यों के अनुसार ऐसा नहीं था। यह दूसरा विचार उन श्लोकों पर आधारित है जिनमें युधिष्ठिर स्वयं अपनी आलोचना करते हैं। युद्ध जीतने के बाद जब युधिष्ठिर रणभूमि में लाखों शवों को देखता है, तब वह अपनी आलोचना करने लगता है और कहता है कि – “दुर्योधन एक अच्छा शासक था और सिंहासन पाने के लिए इतने लोगों के रक्तपात की आवश्यकता नहीं थी।“ यहाँ इस प्रकार के कथनों से इस बात का संकेत कतई नहीं मिलता है कि युधिष्ठिर और दुर्योधन नैतिकता के दृष्टिकोण से एक ही स्तर पर थे। यदि हम महाभारत का पूर्णता से विश्लेषण करें तो नैतिकता और धर्मपरायणता में युधिष्ठिर और दुर्योधन की तुलना करना कतई न्यायसंगत नहीं होगा। निश्चित रुप से युधिष्ठिर दुर्योधन से कई कई गुना अधिक धर्मपरायण राजा थे। अनेक विद्वानों और इतिहासकारों ने भी इन बातों की पुष्टि की है कि युधिष्ठिर का शासनकाल अत्यंत धर्मपरायण था और दुर्योधन का अत्यंत दुर्दांत।
अब हम इस विषय को तीसरे अर्थात एक भक्त के दृष्टिकोण (आध्यात्मिक दृष्टिकोण) से देखते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार जीव का परमधर्म है कि हर परिस्थिति में भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति करे। भगवद्गीता हमें इसी परोधर्म की शिक्षा देती है। युद्ध रोकने के लिए कृष्ण और पाण्डवों ने अपने भरसक प्रयास कर लिए थे। द्यूत-क्रीड़ा के बाद जब पाण्डव वनवास चले गए और उनसे मिलने वहाँ कृष्ण-बलराम आए, तब बलरामजी काफी क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि चूँकि द्यूत-क्रीड़ा एक छल था, पांडवों को तुरंत लौटकर अपना राज्य संभाल लेना चाहिए। यदि कौरव राज्य न लौटाऐं तो उन्हें आक्रमण का भी अधिकार है। युद्ध टालने की दृष्टि से, बलराम जी के इस प्रस्ताव को युधिष्ठिर ने स्वीकार नहीं किया था। द्यूत-क्रीड़ा में छल यह था कि खेल रहे व्यक्ति को ही पाँसे फेंकने थे। लेकिन दुर्योधन की ओर से उसके मामा शकुनि पाँसे फेंक रहे थे और दुर्योधन संपत्ति लगा रहा था, जोकि गलत था। और भी कई बातें गलत हुईं थीं, जो अपनेआप में एक अलग विषय होगा। लेकिन यहाँ यह कहना पर्याप्त होगा कि पाण्डवों का अपना राज्य लेने का अधिकार होते हुए भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तेरह वर्षों का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास भुगता! अज्ञातवास में तो उन्हें चाकरों की भाँति जीना पड़ा जो क्षत्रियों के लिये एकदम लज्जाजनक था। लेकिन शांति बनाये रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इस सबके बाद भी श्रीकृष्ण शांतिदूत बनकर कौरवों के पास गए और मात्र पांच गाँवों की मांग की। इतना सब प्रयास करने पर भी दुर्योधन नहीं माना। अतः युद्ध आवश्यक हो गया।
महाभारत का युद्ध मात्र एक संपत्ति विवाद नहीं था। भीम को विष देना, लाक्षाग्रह षड्यंत्र, द्रौपदी का वस्त्रहरण – ये सब संपत्ति विवाद नहीं था। आधुनिक तथा वैदिक नैतिकता के दृष्टिकोण से भी यदि कोई हत्या की मंशा से आए तो अपने बचाव में शत्रु की हत्या कर देना गलत नहीं माना जाता। कौरवों ने पाण्डवों की हत्या के अनेक प्रयास किए थे।
वैदिक संस्कृति में छह प्रकार के आततायी बताये गए हैं, जिन्हें मारने में कोई दोष नहीं है। पाण्डवों ने महाभारत का युद्ध आत्मरक्षा के लिए किया था। उपरोक्त वर्णित कई कारणों से उनका युद्ध करना उचित था किन्तु उन्होंने अपने पर संयम रखा। कृष्ण भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे किन्तु यह दुर्योधन ही था जो युद्ध चाहता था और उसीके कारण युद्ध हुआ।
यह वास्तविकता कि युद्ध तेरह साल तक टला, यह पाण्डवों के संयम का प्रमाण था और दुर्योधन ने तेरह वर्षों के बाद भी पाण्डवों का राज्य भी उन्हें नहीं लौटाया, यह उसकी दुर्लज्जता का प्रमाण था। महाभारत के युद्ध का उदाहरण हर किसी के साथ युद्ध करने के लिए नहीं दिया जा सकता।
इन सब बातों से स्पष्ट है कि पाण्डव किसी भी दृष्टिकोण से अनैतिक नहीं थे। युद्ध टालने के लिए उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। जब सभी प्रयास विफल हो गए, तब उन्होंने युद्ध करने की ठानी। धर्म के किसी भी दृष्टिकोण से यह अनैतिक नहीं था।
End of transcription.

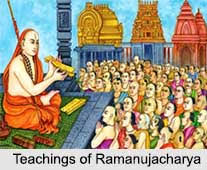
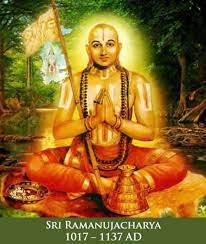



 Today is the appearance anniversary of Sripada Ramanujacharya, the principal acharya in the Sri, or Lakshmi, sampradaya. Srila Prabhupada wrote, “We find great shelter at the lotus feet of Sri Ramanujacharya because his lotus feet are the strongest fort to combat the Mayavadi philosophy.” (letter 22.11.1974) And in the early days of ISKCON in India, before we had Srila Prabhupada’s Bhagavad-gita As It Is in Hindi, Prabhupada would refer people to read the Hindi edition of the Gita with Sri Ramanujacharya’s commentary.
Today is the appearance anniversary of Sripada Ramanujacharya, the principal acharya in the Sri, or Lakshmi, sampradaya. Srila Prabhupada wrote, “We find great shelter at the lotus feet of Sri Ramanujacharya because his lotus feet are the strongest fort to combat the Mayavadi philosophy.” (letter 22.11.1974) And in the early days of ISKCON in India, before we had Srila Prabhupada’s Bhagavad-gita As It Is in Hindi, Prabhupada would refer people to read the Hindi edition of the Gita with Sri Ramanujacharya’s commentary.



 By Gopal Bhatta das
By Gopal Bhatta das

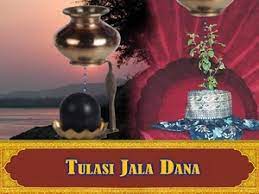








 By Kamalini Devi Dasi
By Kamalini Devi Dasi